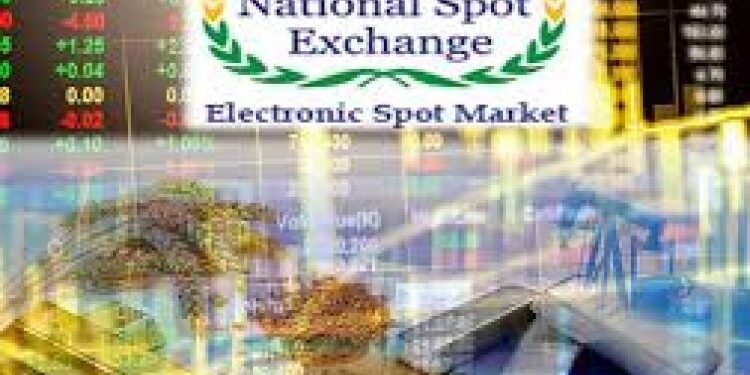सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया, जिससे गर्म राजनीतिक बहस और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हो गए। हाल ही में 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित किया, यह अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बन गया। अब, कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में वक्फ से संबंधित कानून को चुनौती दी है, जिससे गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाते हैं।
अब कानूनी और राजनीतिक हलकों का सामना करना पड़ रहा है: क्या सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा विधिवत रूप से पारित कानून पर हमला किया? इसका जवाब देने के लिए, हमें न्यायपालिका की शक्तियों, संविधान में प्रासंगिक प्रावधानों, और पिछले कानूनों के उदाहरणों को देखने की आवश्यकता है जिन्हें चुनौती दी गई थी और उन्हें पलट दिया गया था।
क्या सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को अमान्य कर सकता है? पता है कि संविधान क्या कहता है
हां, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून को अलग कर सकता है – लेकिन केवल भारत के संविधान द्वारा निर्धारित विशिष्ट परिस्थितियों में।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान की मूल संरचना को परेशान करता है, उसे शीर्ष अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह सिद्धांत न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है। इसलिए, जबकि संसद कानून पारित कर सकती है, उन्हें संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के साथ संरेखित करना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय में संसद कानूनों के उदाहरणों को चुनौती दी गई
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम पहली बार नहीं है जब किसी कानून को न्यायिक रूप से चुनौती दी गई है। उनकी संवैधानिक वैधता के लिए कई महत्वपूर्ण संसद-पास किए गए कानूनों पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मामले हैं:
आधार अधिनियम (2016): अनुच्छेद 21 (गोपनीयता का अधिकार) का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बरकरार रखा, लेकिन निजी कंपनियों द्वारा इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया।
NJAC अधिनियम (2014): नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन अधिनियम 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता को कम करने के लिए, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल करने के लिए मारा गया था।
चुनावी बांड योजना (2017): हाल ही में, अदालत ने इसे असंवैधानिक और दाताओं की पहचान के प्रकटीकरण को निर्देशित किया।
फार्म लॉज (2020): व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद अदालत द्वारा इन्हें रोका गया, और अंततः संसद द्वारा वापस ले लिया गया।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019): हालांकि चुनौती दी गई थी, इस कानून को अदालत द्वारा बरकरार रखा गया था।
ये उदाहरण सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान की रक्षा करने और यहां तक कि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रतिबिंबित करते हैं जो इसके मूल सिद्धांतों के साथ असंगत हैं।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम: कानूनी और राजनीतिक विवाद क्या है?
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को ट्रिगर किया है, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों से। WAQF कानून, जो इस्लामी बंदोबस्तों के प्रबंधन से संबंधित है, कई कारणों से आग में आ गया है:
धार्मिक स्वायत्तता: याचिकाकर्ताओं का दावा है कि गैर-मुस्लिमों को WAQF बोर्डों में नियुक्त करना संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
दाता प्रतिबंध: आलोचकों का तर्क है कि 5 वर्षों से विश्वास में रहने वाले मुसलमानों को वक्फ दाताओं को प्रतिबंधित करना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।
तुलनात्मक उपचार: याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल किया कि हिंदू और सिख धार्मिक गुणों को सरकार द्वारा समान रूप से प्रबंधित क्यों नहीं किया जाता है, यह तर्क देते हुए कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम संपत्तियों को गलत तरीके से मानता है।
राजनीतिक विरोध: कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और जेएमएम जैसी दलों ने धार्मिक और संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए, कानून का खुले तौर पर विरोध किया है।
इस मामले को पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जा रहा है, और इसके परिणाम में दूरगामी कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।
यदि सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को रद्द कर देता है तो क्या होता है? संसद के विकल्पों को समझना
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को रद्द कर दे, संसद के पास अभी भी विकल्प हैं। उदाहरण के लिए, 1961 में आरक्षण से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, लेकिन संसद ने एक अध्यादेश लाया और अदालत के फैसले को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया। उन्होंने नए खंड जोड़े और कानून को फिर से प्रस्तुत किया।
इससे पता चलता है कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय एक कानून को रद्द कर देता है, संसद परिवर्तनों के साथ कानून का एक नया संस्करण ला सकती है, या इसे जीवित रखने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है।